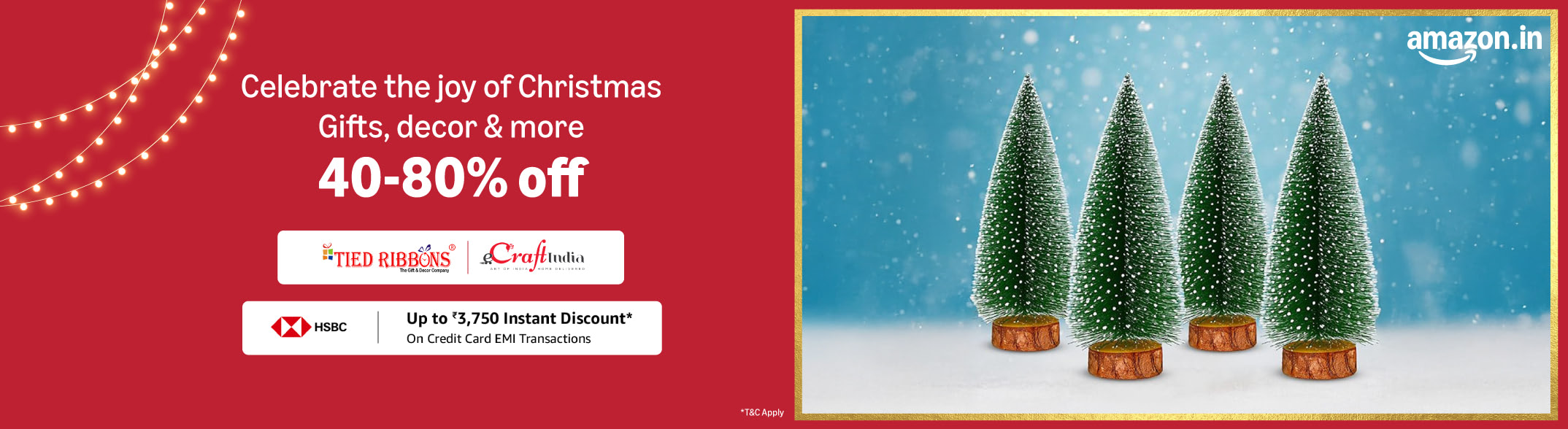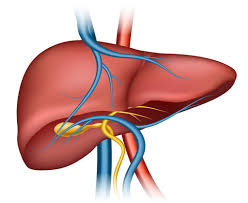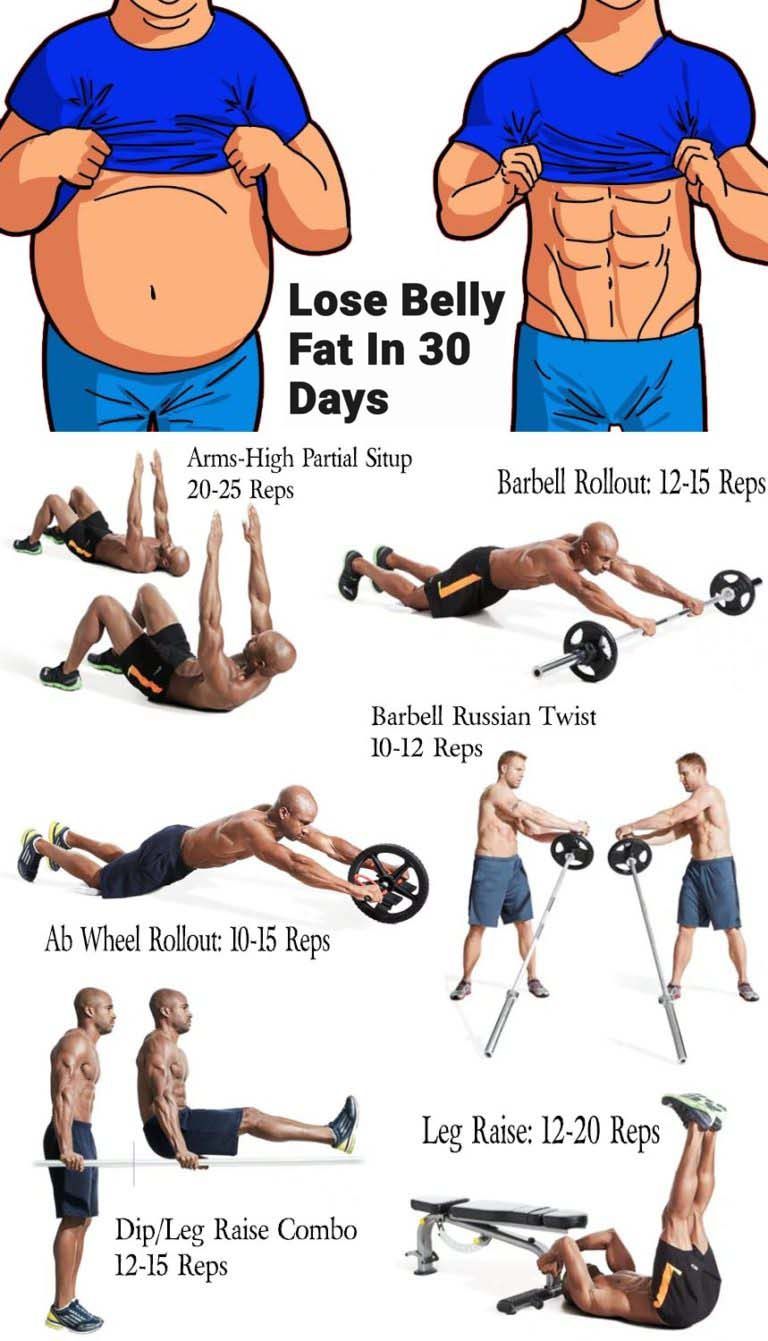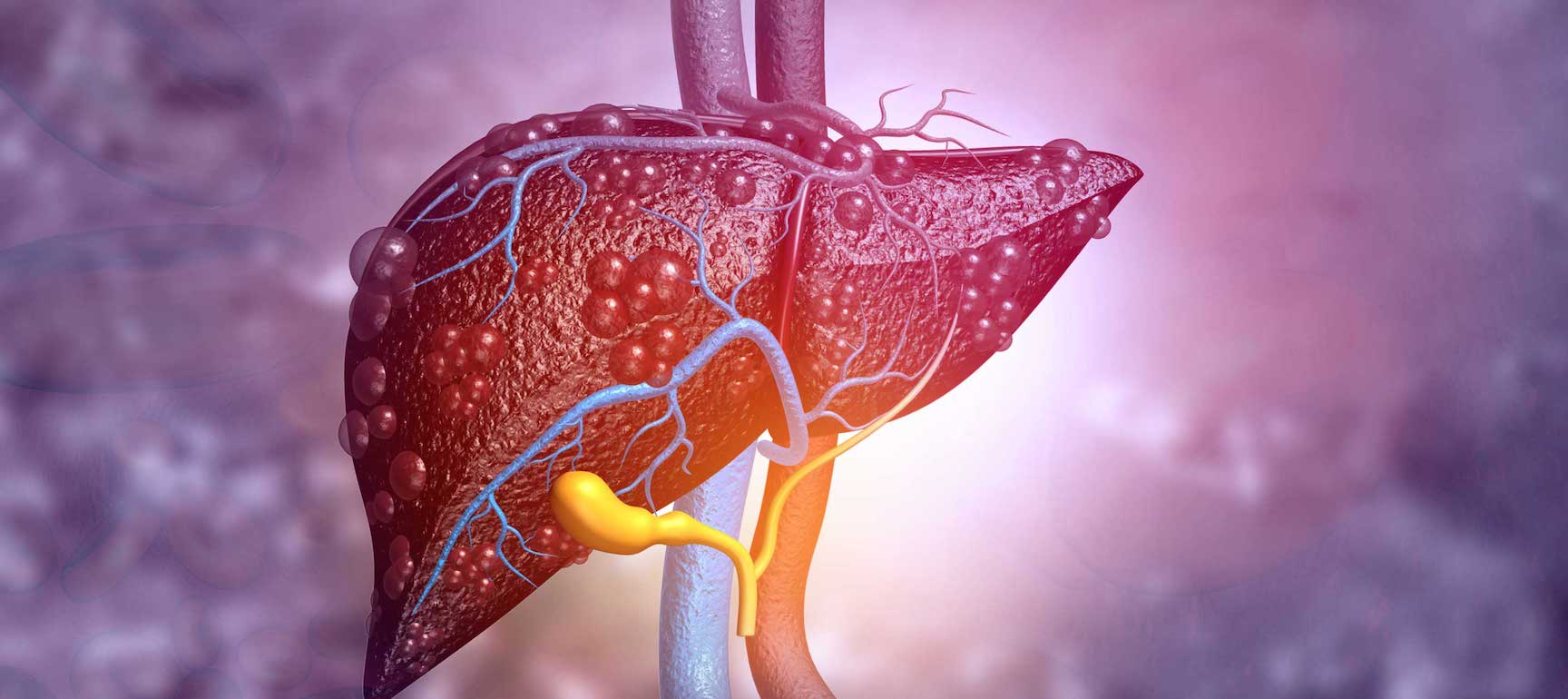स्ट्रोक पुनर्वास को मेडिकल मुख्यधारा में लाना अब कोई विकल्प नहीं — यह एक जरूरत है
- byAman Prajapat
- 29 October, 2025

जब कोई व्यक्ति Stroke अर्थात् “मस्तिष्क घटना” से गुज़रता है, तो अक्सर हम केवल “अचानक हुआ, अस्पताल गया, इलाज हुआ” ही सोच लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि घटना के तुरंत बाद चिकित्सा सेवा यानी थ्रोम्बॉलिसिस, स्ट्रोक यूनिट में भर्ती आदि जितने महत्वपूर्ण हैं — उतना ही, अगर चुपचाप लेकिन दृढ़ता से, पुनर्वास प्रक्रिया है। पुनर्वास यानी वो सफर जहाँ व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी पहले की जिंदगी, गति, भाषा, हाथ-पैर की गतिविधियाँ वापस पाने की कोशिश करता है।
और यह सफर अक्सर अधूरा रह जाता है — खासकर भारत में।
भारत में इस दिशा में कुछ अध्ययन बताते हैं:
एक राष्ट्रीय-स्तरीय सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में लगभग 1.8 % आबादी को स्ट्रोक का निदान हुआ है, लेकिन उनमें से केवल करीब 40 % ने भौतिक चिकित्सा या व्यावसायिक चिकित्सा (physical/occupational therapy) जैसी पुनर्वास सेवाएँ लीं।
पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता, जागरूकता, आर्थिक पहुंच — ये सभी बड़ी बाधाएँ हैं।
सुधार-प्रभाव वाले शोध भी बताते हैं कि अगर समय पर और सही-प्रकार से पुनर्वास मिले तो जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।
तो यहाँ हम विस्तार से देखेंगे — क्यों पुनर्वास मुख्यधारा में लाना ज़रूरी है, कौन-सी चुनौतियाँ खड़ी हैं, और आगे क्या किया जा सकता है।
1. पुनर्वास को मुख्यधारा में लाने का अर्थ
“मुख्यधारा” यानी — अस्पताल में भर्ती, तुरंत इलाज से निकलकर — निरंतर देखभाल, थैरेपी, घरेलू और सामुदायिक स्तर पर सक्रिय समर्थन शामिल होना। सिर्फ “आप ठीक हो गए” कह देना पर्याप्त नहीं। स्ट्रोक के बाद जीवन नए प्रारूप में होता है — व्यक्ति को चलना, बात करना, खाना-पीना, सामाजिक जुड़ाव — सब कुछ फिर-से सीखना पड़ता है। यदि पुनर्वास नहीं होगा, तो यह सफर अधूरा रहेगा।
और जब पुनर्वास मुख्यधारा में नहीं होगा, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं — रोगी जीवन में लंबे समय तक विकलांगता के साथ रह सकता है, परिजनों पर बोझ बढ़ता है, स्वास्थ्य-व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है।
2. समस्या का आकलन — भारत का परिदृश्य
भारत में पुनर्वास की स्थिति — सीधी और कठोर है। कुछ आंकड़ियाँ बताती हैं:
भारत में लगभग 1,251 स्ट्रोक पुनर्वास केंद्र हैं, जबकि आबादी करीब 1.46 अरब है — यानि लगभग हर 11.7 लाख लोगों पर एक केंद्र।
पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पर्याप्त नहीं हैं।
ग्रामीण इलाकों एवं छोटे-शहरों में पुनर्वास सुविधाएँ बहुत कम हैं — अधिकांश केंद्र महानगरों और बड़े शहरों में केंद्रित हैं।
रोगी स्वयं और उनके परिवारों को अक्सर पुनर्वास के विकल्पों के बारे में जानकारी नहीं होती — क्या थैरेपी होगी, कब शुरू होगी, कितने समय तक चलेगी, कौन-से विशेषज्ञ होंगे — यह अस्पष्ट रहता है।
इस तरह, पुनर्वास को मुख्यधारा में नहीं लाने का परिणाम — “इलाज खत्म हुआ, अब छोड़ दो” जैसी मानसिकता — बन जाता है। लेकिन यह मानसिकता अब चलने योग्य नहीं है।
3. पुनर्वास न होने के दुष्परिणाम
यदि पुनर्वास समय पर और सही तरीके से न हो — तो क्या होगा? कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं:
चलने-फिरने, हाथ-पैर उपयोग करने, बोलने, निगलने जैसी गतिविधियों में स्थायी कमी आ सकती है।
रोगी की आत्म-निर्भरता बहुत कम हो जाती है, सामाजिक जीवन सीमित हो जाता है।
परिवारों पर देखभाल का बोझ बहुत बढ़ जाता है — आर्थिक, भावनात्मक, सामाजिक।
अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद पुनरावृत्ति (recurrence) या दूसरी स्वास्थ्य जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है।
स्वास्थ्य-व्यवस्था में लागत बढ़ती है — लंबे समय तक देखभाल, पुनः भर्ती आदि।
उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि चेंन्नई-आधारित स्ट्रोक मरीजों एवं उनके देखभालकर्ताओं ने 70 % से अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता जताई और 80 % से अधिक ने सूचना-वंचितता की समस्या बताई।
4. पुनर्वास को मुख्यधारा में लाने की चुनौतियाँ
यह आसान काम नहीं है। मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
संरचना एवं संसाधन: पर्याप्त पुनर्वास केंद्र, योग्य फिजियोथेरेपिस्ट, ओक्युपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कमी है।
आर्थिक बाधाएँ: अधिकांश स्वास्थ्य बीमा और कॉर्पोरेट स्वास्थ्य योजनाएँ पुनर्वास को पर्याप्त कवर नहीं करतीं। इससे रोगी व परिवार को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।
जागरूकता की कमी: चिकित्सक, मरीज, परिजन — तीनों में ही पुनर्वास को लेकर जागरूकता कम है। कई बार चिकित्सक स्ट्रोक के बाद पुनर्वास के विकल्प नहीं बताते।
प्रारंभिक हस्तक्षेप में देरी: स्ट्रोक के बाद “स्वर्ण विंडो” (पहले कुछ सप्ताह-महीने) बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि इस दौरान थैरेपी शुरू नहीं हुई, तो रिकवरी की संभावना कम हो जाती है।
भौगोलिक असमानता: ग्रामीण-और दूरस्थ इलाकों में पुनर्वास सुविधाएँ बहुत कम हैं। वहाँ पहुंचना, खर्च करना कठिन है।
नीति-प्रोटोकॉल की कमी: भारत में स्ट्रोक के बाद पुनर्वास के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा-निर्देश पर्याप्त नहीं हैं।

5. समाधान-केन्द्रित दृष्टिकोण
तो अब बात करते हैं — “क्या करें?” — क्योंकि सिर्फ समस्या गिना लेने से काम नहीं होगा। हमें पुराने तरीके को छोड़ कर, एक नया-पुराना (traditionally rooted) दृष्टिकोण अपनाना होगा — जहाँ पुनर्वास को “इलाज का हिस्सा” माना जाए, न कि “जिम्मेदारी खत्म होने के बाद” का विकल्प। नीचे कुछ सुझाव दिए हैं:
समय पर थैरेपी शुरू करें: स्ट्रोक के बाद जितनी जल्दी संभव हो, पुनर्वास शुरू हो। अस्पताल में ही डिस्चार्ज से पहले पुनर्वास टीम से संपर्क सुनिश्चित हो।
पुनर्वास को अस्पताल-पथ में शामिल करें: इलाज खत्म होते ही “ठीक हो गए” कह देना पर्याप्त नहीं। अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट के बाद पुनर्वास यूनिट, फिजियोथेरेपी, ओक्युपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी — ये सब एकीकृत हों।
बहु-विषयक टीम बनाएँ: न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओक्युपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोविज्ञानी — मिलकर काम करें।
घरेलू और समुदाय-स्तरीय पुनर्वास: अस्पताल से घर लौटने के बाद भी निरंतर समर्थन हो। टेली-थेरेपी, मोबाइल-ऐप आधारित निर्देश, घर-आधारित व्यायाम-प्रोटोकॉल आदि विकसित करें।
आर्थिक कवरेज और नीति-समर्थन: स्वास्थ्य बीमा में पुनर्वास को शामिल किया जाए। सरकार-नीति द्वारा पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार हो। पुनर्वास-केन्द्रों का निर्माण विशेष रूप से ग्रामीण-दूरस्थ इलाकों में हो।
जागरूकता एवं शिक्षा बढ़ाएँ: रोगी-परिजन को स्ट्रोक के बाद पुनर्वास की महत्ता समझाएँ। चिकित्सकों को भी पुनर्वास की दिशा में प्रशिक्षित करें।
माप-दंड एवं दिशा-निर्देश बनाएँ: राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रोक के बाद पुनर्वास के लिए मानक निर्माण हो — कब शुरू हो, कितने समय तक चले, कौन-सी टीम जिम्मेदार हो, आदि।
प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सस्ते उपकरण, टेली-रेहैबिलिटेशन, एआई-सहायता उपकरण — जैसे भारत में कुछ अध्ययन हुए हैं।
6. मुख्यधारा लाने से क्या मिलेगा?
जब हम पुनर्वास को मुख्यधारा में लाएंगे, तो यह सिर्फ एक सेवा नहीं बढ़ेगी — बल्कि कुछ गहरे परिवर्तन होंगे:
स्ट्रोक से जिंदा निकलने वाले व्यक्तियों की गुणवत्ता ज़िंदगी सुधार जाएगी — वे आत्म-निर्भर होंगे, सामाजिक रूप से जुड़े रहेंगे।
परिजन-बोझ कम होगा, सामाजिक-आर्थिक नुकसान कम होगा।
स्वास्थ्य-व्यवस्था पर लंबी अवधि में दबाव कम होगा — बार-बार अस्पताल जाना, पुनः भर्ती होना घटेगा।
नीति-निर्माता, चिकित्सक और समाज में स्वास्थ्य देखभाल की ‘पूरक’ (rehabilitation) भागीदारी बढ़ेगी — यह दिखाएगा कि इलाज का मतलब सिर्फ “बचे रहना” नहीं, बल्कि “जीना” भी है।
भारत में ‘पुनर्वास’-संबंधी रुकावटें कम होंगी और ‘उपचार के बाद की देखभाल’ को एक विचारशील अंग बना दिया जाएगा।
7. निष्कर्ष
तो भाई/बहन, बात यह है — यदि हम पुराने-पुराने तरीके से काम करते रहेंगे — सिर्फ पलमपाइमेंट (acute care) पर जोर देंगे और उसके बाद “चलो घर जाओ” कह देंगे — तो स्ट्रोक की लड़ाई आधी ही जीती होगी। लेकिन अगर हम पुनर्वास को इलाज का-अटूट हिस्सा मान लें, उसे प्राथमिकता दें, समय पर शुरू करें, टीम-बनाएँ, नीति-समर्थन दें — तब हम सच में स्ट्रोक-मार्ग पर खड़े लोगों को “वापस जीवन” दे सकते हैं।
यह कोई नया आइडिया नहीं है — लेकिन यह समय आ गया है कि इसे मुख्यधारा बना दिया जाए। पुराने-जमाने की दवा-केंद्रित सोच में ‘चंगा हो गया’ कह देना काफी नहीं। हमें देखना है कि वो व्यक्ति चल सके, बात कर सके, काम कर सके, मुस्कुरा सके — और पुराने-स्वागत योग्य जीवन को फिर-से पाए।
Note: Content and images are for informational use only. For any concerns, contact us at info@rajasthaninews.com.
40 के बाद शर्ट से बा...
Related Post
Hot Categories
Recent News
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.